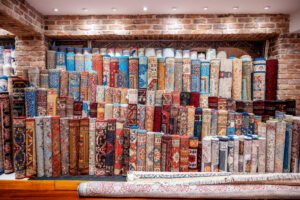उत्तर प्रदेश (UP) ने अपने धर्मांतरण विरोधी कानून को और अधिक कठोर कैसे बनाया है? | व्याख्या
1 min read
उत्तर प्रदेश (UP) विधानसभा ने 30 जुलाई को मूल 2021 धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया था। आलोचना का विषय कौन सी विशेषताएँ हैं? यह कानून भाजपा शासित राज्यों के समान कानूनों से किस तरह अलग है? आगे क्या होगा?
अब तक की कहानी: उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 30 जुलाई को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया, जिसने 2021 के मूल धर्मांतरण विरोधी कानून में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए इसके प्रावधानों को और अधिक कठोर बना दिया, और आलोचकों का कहना है कि इसका दुरुपयोग होने की संभावना है। 2017 से, कई भाजपा शासित राज्यों ने विवाह, छल, जबरदस्ती या प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए या संशोधित किए हैं। इन उपायों का उद्देश्य स्पष्ट रूप से “लव जिहाद” का मुकाबला करना है – एक सिद्धांत, जिसे मुख्य रूप से हिंदुत्व समूहों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, जो आरोप लगाता है कि अंतर-धार्मिक विवाह संभावित जबरन धर्मांतरण के स्थल हैं।
अब तक की कहानी: उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 30 जुलाई को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया, जिसने 2021 के मूल धर्मांतरण विरोधी कानून में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए इसके प्रावधानों को और अधिक कठोर बना दिया, और आलोचकों का कहना है कि इसका दुरुपयोग होने की संभावना है। 2017 से, कई भाजपा शासित राज्यों ने विवाह, छल, जबरदस्ती या प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए या संशोधित किए हैं। इन उपायों का उद्देश्य स्पष्ट रूप से “लव जिहाद” का मुकाबला करना है – एक सिद्धांत, जिसे मुख्य रूप से हिंदुत्व समूहों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, जो आरोप लगाता है कि अंतर-धार्मिक विवाह संभावित जबरन धर्मांतरण के स्थल हैं।
यह भी पढ़ें: मध्यकालीन सोच: उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून और उसके संशोधनों पर
यह संशोधन क्यों प्रस्तावित किया गया?
विधेयक के कारणों के अनुसार, अवैध धर्मांतरण के कारण जनसांख्यिकीय परिवर्तन में “विदेशी और राष्ट्र-विरोधी तत्वों और संगठनों” की कथित “संगठित और सुनियोजित” संलिप्तता के कारण मौजूदा कानून को “जितना संभव हो सके उतना कठोर” बनाने की आवश्यकता है। इसमें आगे कहा गया है कि 2021 अधिनियम के दंडात्मक प्रावधान नाबालिगों, विकलांग व्यक्तियों, मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, महिलाओं और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों में “धार्मिक धर्मांतरण और सामूहिक धर्मांतरण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे”।
जबकि कानून की संवैधानिक वैधता सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन है, राज्य सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि 1 जनवरी 2021 से 30 अप्रैल 2023 के बीच अधिनियम के तहत 427 मामले दर्ज किए गए, जिसके परिणामस्वरूप 833 गिरफ्तारियां हुईं।
क्या इससे दंड में वृद्धि होगी?
सरकार ने कानून के तहत सभी अपराधों के लिए जेल की अवधि और जुर्माने को बढ़ा दिया है। पहले, अवैध धर्मांतरण के दोषी व्यक्ति को न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष की जेल की सजा के साथ-साथ 15,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता था। संशोधित विधेयक के तहत, ऐसे अपराधों के लिए न्यूनतम कारावास की अवधि बढ़ाकर 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष कर दी गई है। इसके अलावा, जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है।
नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्ति के अवैध धर्मांतरण के लिए सजा की अवधि 2-10 साल से बढ़ाकर 5-14 साल कर दी गई है। न्यूनतम जुर्माना भी 25,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है।
विधेयक में सामूहिक धर्मांतरण के लिए दंड को भी कड़ा किया गया है। पहले, दोषी पाए जाने वालों को न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 10 साल की जेल की सजा होती थी। अब न्यूनतम सजा को बढ़ाकर 7 साल और अधिकतम 14 साल कर दिया गया है, साथ ही जुर्माना भी दोगुना करके 1 लाख रुपये कर दिया गया है।
संशोधन में अपराधों की दो नई श्रेणियां भी शामिल की गई हैं। सबसे पहले, धारा 5 में नई जोड़ी गई उप-धारा के अनुसार, गैरकानूनी धर्मांतरण के उद्देश्य से “विदेशी” धन या “अवैध संस्थानों” से धन प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए न्यूनतम 7 वर्ष की जेल अवधि, जिसे 14 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, अनिवार्य है। उन्हें 10 लाख रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। दूसरा, यदि अभियुक्त किसी व्यक्ति को उसके जीवन या संपत्ति के लिए भय पैदा करता है, हमला करता है या बल का प्रयोग करता है, शादी का वादा करता है या उकसाता है, किसी नाबालिग, महिला या व्यक्ति को तस्करी करने या अन्यथा बेचने के लिए साजिश करता है या प्रेरित करता है, तो उन्हें न्यूनतम 20 साल के कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। अदालतों को पीड़ितों को उचित मुआवजा देने की भी आवश्यकता होती है, जिसका भुगतान अभियुक्तों द्वारा किया जाना चाहिए। यह मुआवजा 5 लाख रुपये तक हो सकता है और लगाए गए किसी भी जुर्माने के अतिरिक्त है।
आपराधिक शिकायत कौन दर्ज करा सकता है?
मूल अधिनियम की धारा 4 के तहत, केवल “कोई भी पीड़ित व्यक्ति” या “उसके माता-पिता, भाई, बहन या कोई अन्य व्यक्ति जो उसके साथ रक्त, विवाह या गोद लेने से संबंधित है” को गैरकानूनी धर्मांतरण के लिए आपराधिक शिकायत दर्ज करने का अधिकार था। इस प्रतिबंध के बावजूद, पुलिस अधिकारी कथित तौर पर दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं और निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधियों सहित अन्य अनधिकृत तीसरे पक्षों के इशारे पर एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दे रहे थे। इसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को एक से अधिक अवसरों पर यह स्पष्ट करने के लिए प्रेरित किया कि ऐसी शिकायतें केवल पीड़ित व्यक्ति या उनके रिश्तेदारों द्वारा ही दर्ज की जा सकती हैं।
हालाँकि, संशोधन अब ऐसी तीसरे पक्ष की शिकायतों को वैधता प्रदान करता है। संशोधित प्रावधान में कहा गया है कि “कोई भी व्यक्ति” आपराधिक प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले नए कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) के अध्याय 13 के तहत दिए गए तरीके से अधिनियम के किसी भी उल्लंघन से संबंधित एफआईआर दर्ज कर सकता है। यह अध्याय किसी अपराध के होने के बारे में सूचना मिलने पर जांच करने के लिए पुलिस अधिकारियों की शक्तियों से संबंधित है।
जमानत के प्रावधानों के बारे में क्या?
संशोधन में ज़मानत की कठोर “जुड़वां शर्तें” पेश की गई हैं , जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 और गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 जैसे क़ानूनों के तहत हैं। गैरकानूनी धर्मांतरण से संबंधित सभी अपराध अब संज्ञेय और गैर-जमानती हैं और उन पर केवल सत्र न्यायालय या उच्च न्यायिक मंचों द्वारा ही निर्णय लिया जा सकता है।
संशोधित धारा 7 के तहत, किसी अभियुक्त को पहले सरकारी वकील को जमानत आवेदन का विरोध करने का अवसर दिए बिना जमानत नहीं दी जा सकती। इसके अलावा, अगर सरकारी वकील ऐसी दलील का विरोध करता है, तो सत्र न्यायालय केवल तभी जमानत दे सकता है जब “यह मानने के लिए उचित आधार हों कि [आरोपी] ऐसे अपराध का दोषी नहीं है” और यह कि जमानत पर रिहा होने पर उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। अभियुक्त पर सबूत का उल्टा बोझ इस प्रावधान को कठोर बनाता है, जिससे किसी के लिए भी मुकदमा पूरा होने तक जमानत प्राप्त करना लगभग असंभव हो जाता है।
अन्य धर्मांतरण विरोधी कानूनों की तुलना में यह कैसा है?
उत्तर प्रदेश के अलावा, ओडिशा, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में दशकों से धर्मांतरण विरोधी कानून हैं, जबकि छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड ने हाल ही में ऐसे कानून लागू किए हैं। 2022 में, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने कर्नाटक में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण अधिनियम पेश किया , जिसे अंततः पिछले साल कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने खत्म कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने भी ऐसा कानून बनाने में रुचि दिखाई है।
इनमें से ज़्यादातर कानूनों के तहत धर्म परिवर्तन करने का इरादा रखने वाले या धर्म परिवर्तन में मदद करने वाले लोगों को सरकार को सूचित करना ज़रूरी है। मध्य प्रदेश में, धर्म परिवर्तन को वैध बनाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को 60 दिन पहले “धर्म परिवर्तन के इरादे की घोषणा” करना अनिवार्य है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 30 दिन पहले नोटिस देना ज़रूरी है। इसके विपरीत, उत्तर प्रदेश में न केवल 60 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है, बल्कि धर्म परिवर्तन के पीछे असली इरादे का पता लगाने के लिए मजिस्ट्रेट को पुलिस जांच भी करवानी होगी।
एक और उल्लेखनीय अंतर यह है कि अन्य राज्य पीड़ित व्यक्ति या उनके निकटतम परिवार- जैसे माता-पिता या भाई-बहन तक ही एफआईआर दर्ज करने को सीमित रखते हैं, इस प्रकार संभावित निहित स्वार्थ वाले तीसरे पक्ष को कोई कानूनी कार्रवाई शुरू करने से बाहर रखा जाता है। मध्य प्रदेश में, पुलिस शिकायत दर्ज करने से पहले अभिभावकों को भी अदालत की मंजूरी लेनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश में, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के पद से नीचे के अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना अभियोजन शुरू नहीं किया जा सकता है।
अंतरिम रिहाई सुनिश्चित करने के लिए उच्च सीमा निर्धारित करने वाली “जमानत की दोहरी शर्तें” भी कुछ अन्य राज्य कानूनों में अनुपस्थित हैं। हालाँकि, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य सबूत के रिवर्स बर्डन को अनिवार्य करते हैं, जिसके तहत आरोपी को यह साबित करना होता है कि कोई गैरकानूनी धर्मांतरण नहीं हुआ है। सजा की मात्रा के संबंध में, अन्य राज्यों के किसी भी कानून में आजीवन कारावास का प्रावधान नहीं है; इसके बजाय, जेल की सजा 2 से 10 साल के बीच होती है।
आगे क्या होता है?
संशोधन की संवैधानिक वैधता को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दिए जाने की संभावना है। भाजपा शासित राज्यों द्वारा बनाए गए मूल कानून और इसी तरह के अन्य धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं का एक समूह पहले से ही भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष लंबित है। हालाँकि, इन याचिकाओं को अप्रैल 2023 से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है, जिससे वे प्रभावी रूप से अधर में लटकी हुई हैं।
इस बीच, मई में, गैरकानूनी धार्मिक रूपांतरण के आरोप को रद्द करने की मांग करने वाले एक अलग मामले की सुनवाई करते हुए, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने टिप्पणी की थी कि 2021 अधिनियम के कुछ प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करते प्रतीत होते हैं, जो धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।